- Home
- HISTORY
- _ANCIENT INDIA
- __ARTICLE
- __MCQ
- __Q & A
- _MEDIEVAL INDIA
- __ARTICLE
- __MCQ
- __Q & A
- _MODERN INDIA
- __ARTICLE
- __MCQ
- __Q & A
- _WORLD HISTORY
- __MCQ
- GEOGRAPHY
- _INDIA GEOGRAPHY
- __ARTICLE
- __MCQ
- __Q & A
- _WORLD GEOGRAPHY
- __ARTICLE
- __MCQ
- __Q & A
- SCIENCE
- _PHYSICS
- __ARTICLE
- __MCQ
- __Q & A
- _CHEMISTRY
- __ARTICLE
- __MCQ
- __Q & A
- _BIOLOGY
- __ARTICLE
- __MCQ
- __Q & A
- POLITY
- _ARTICLE
- _MCQ
- _Q & A
- ECONOMY
- _ARTICLE
- _MCQ
- _Q & A
- COMPUTER
- _ARTICLE
- _MCQ
- _Q & A
- MORE SUBJECTS
- _HINDI
- __ARTICLE
- __MCQ
- __Q & A
- _CHILD DEVELOPMENT
- __ARTICLE
- __MCQ
- __Q & A
- TREND
भूगोल का अर्थ, परिभाषाएँ, विकास और शाखाएँ (Meaning, definitions, development and branches of geography)
GKBIGBOSS
गुरुवार, अप्रैल 10, 2025
↪ भौतिक भूगोल का संबंध पृथ्वी के भौतिक तत्वों के अध्ययन से है। भौतिक भूगोल भौतिक पर्यावरण और पृथ्वी के भौतिक पर्यावरण में परिवर्तन लाने वाली विभिन्न गतिविधियों से संबंधित है। दूसरी ओर, 'मानव भूगोल' पृथ्वी पर मनुष्य का अध्ययन करता है। मानव भूगोल पृथ्वी और मनुष्य के बीच संबंधों की एक नई समझ देता है, जिसमें पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियमों और पृथ्वी पर रहने वाले जीवों के आपसी संबंधों का अधिक व्यापक ज्ञान शामिल है।
↪ 'भूगोल' (Geography) दो ग्रीक शब्दों 'geo' (जिसका अर्थ है 'पृथ्वी') और 'grapho' (जिसका अर्थ है 'वर्णन') से मिलकर बना है जिनका संयुक्त अर्थ है - "पृथ्वी का वर्णन"। पृथ्वी को हमेशा से ही मनुष्यों के निवास स्थान के रूप में देखा जाता रहा है और इस दृष्टिकोण से, विद्वान भूगोल को "पृथ्वी का मनुष्यों के निवास स्थान के रूप में वर्णन" के रूप में परिभाषित करते हैं।
↪ दूसरे शब्दों में, "भूगोल व्यापक पैमाने पर सभी भौतिक और मानवीय तथ्यों की अंतःक्रियाओं और इन अंतःक्रियाओं से उत्पन्न भू-आकृतियों का अध्ययन करता है। भूगोल बताता है कि मानव और प्राकृतिक गतिविधियाँ कैसे, क्यों और कहाँ उत्पन्न होती हैं और ये गतिविधियाँ एक-दूसरे से कैसे जुड़ी हुई हैं।
↪ भूगोल का एक अन्य पहलू क्षेत्रीय विविधता के कारकों या कारणों को समझने से संबंधित है, कि कैसे सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और जनसांख्यिकीय कारक भौतिक भू-आकृतियों को बदल रहे हैं और कैसे मानवीय हस्तक्षेप के परिणामस्वरूप पुराने स्थल नष्ट हो रहे हैं और नए भू-आकृतियों का निर्माण हो रहा है।
↪ संसाधनों और पर्यावरणीय प्रक्रियाओं के सतत उपयोग के बारे में अधिक जानने और यह समझने के लिए कि भूमि उपयोग नियोजन समस्याओं को हल करने में कैसे मदद कर सकता है, भूगोल का अध्ययन आवश्यक है।
↪ भूगोलवेत्ता प्रारंभ में भूगोल की व्याख्या वर्णनात्मक ढंग से करते थे, बाद में यह विश्लेषणात्मक भूगोल के रूप में विकसित हो गया। आज यह विषय न केवल वर्णन करता है बल्कि विश्लेषण एवं भविष्यवाणी भी करता है।
↪ भूगोल का नामकरण तथा उसे प्राथमिक स्तर पर व्यवस्थित रूप देने का श्रेय यूनान के निवासियों को है।
↪ इरैटोस्थनीज ( 276-194 ई. पू. ) प्रथम यूनानी वैज्ञानिक था, जिसने भूगोल के लिए 'ज्योग्राफिका' शब्द का प्रयोग किया। इन्होंने ही पृथ्वी का सर्वप्रथम सही मापन किया। इन्हें 'व्यवस्थित भूगोल का जनक' कहा जाता है।
↪ हिकेटियस को 'भूगोल का पिता' कहा जाता है, क्योंकि, इन्होंने सर्वप्रथम अपनी पुस्तक 'जेस पीरियोडस' अर्थात "पृथ्वी का विवरण" में भौगोलिक तत्वों का वर्णन किया था। हेकेटियस ने भूमि को महासागरों से घिरा हुआ माना तथा दो महाद्वीपों का ज्ञान दिया।
↪ अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट को 'आधुनिक भूगोल का जनक' कहा जाता है। उन्होंने आधुनिक भूगोल का विकास वैज्ञानिक एवं दार्शनिक आधार पर किया। 'कॉसमॉस' हम्बोल्ट की प्रसिद्ध कृति है। वह मानचित्र पर 'समताप रेखा' दिखाने वाले पहले व्यक्ति थे।
↪ पौलीडोनियम को ' भौतिक भूगोल का जनक' कहा जाता है।
↪ कार्ल-ओ-सावर को 'सांस्कृतिक भूगोल का जनक' कहा जाता है।
↪ गणितीय भूगोल के संस्थापक थेल्स व एनेक्सीमीण्डर को माना जाता है।
↪ सर्वप्रथम विश्व का मानचित्र अनेक्जीमोडर ने बनाया था।
↪ सर्वप्रथम विश्व ग्लोब मार्टिन बैहम ने बनाया था।
↪ टॉलमी ने मानचित्र बनाने तथा स्थानों की स्थिति के लिए अक्षांश तथा देशांतर की जानकारी दी।
↪ यूनानी दार्शनिक अरस्तू ने सर्वप्रथम विश्व को गोलाभ कहा।
↪ स्ट्रैबो के अनुसार, "भूगोल एक स्वतंत्र विषय है जिसका उद्देश्य लोगों को विश्व, खगोलीय पिंडों, भूमि, महासागरों, प्राणियों, पौधों, फलों और पृथ्वी की सतह पर दिखाई देने वाली अन्य चीजों से अवगत कराना है।"
↪ टॉलेमी के अनुसार, “भूगोल स्वर्ग में पृथ्वी का प्रतिबिम्ब देखने का विज्ञान है।”
↪ रिचर्ड हार्टशॉर्न के अनुसार, "भूगोल का उद्देश्य पृथ्वी के क्षेत्रीय/ब्रह्मांडीय अंतरों का वर्णन और व्याख्या करना है।"
↪ कार्ल रिटर के अनुसार, "भूगोल वह विज्ञान है जिसमें पृथ्वी को एक स्वतंत्र ग्रह के रूप में मान्यता दी जाती है और इसकी सभी विशेषताओं, घटनाओं और इसके अंतर्संबंधों का अध्ययन किया जाता है।"
↪ प्राचीन काल में पृथ्वी से संबंधित अधिकांश जानकारी अन्य विषयों के विद्वानों से प्राप्त की जाती थी, जैसे - 'हिप्पोक्रेट्स' ने मनुष्य पर पर्यावरण के प्रभाव का वर्णन किया है। अरस्तु ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक "पॉलिटिक्स" में राज्य के गठन पर भौतिक कारकों के प्रभाव को स्पष्ट किया है।
↪ 18वीं शताब्दी में सजीव भौगोलिक विवरणों का लेखन नए भौगोलिक क्षेत्रों और समुद्री मार्गों की खोज के साथ शुरू हुआ, क्योंकि यूरोपीय उपनिवेशों की विजय इनसे जुड़ी हुई थी।
↪ 19वीं शताब्दी की शुरुआत में भूगोल का स्वतंत्र अध्ययन शुरू हुआ, जिसमें 'ए.वी. हम्बोल्ट' और 'कार्ल रिटर' ने अतुलनीय योगदान दिया है। भूगोल को 19वीं शताब्दी में ही अध्ययन के एक स्वतंत्र विषय के रूप में मान्यता दी गई थी।
↪ 20वीं सदी के आरंभ में भूगोल का अध्ययन 'मनुष्य और पर्यावरण' के पारस्परिक संबंधों के रूप में आरंभ हुआ। इसके अध्ययन से संबंधित भूगोलवेत्ताओं के दो समूह बने, जिनकी अपनी-अपनी विचारधाराएँ थीं -
भूगोल अध्ययन का एक अंतःविषय है। प्रत्येक विषय का अध्ययन किसी न किसी दृष्टिकोण के अनुसार किया जाता है। भूगोल के अध्ययन के प्रमुख दृष्टिकोण इस प्रकार हैं:-
व्यवस्थित दृष्टिकोण के आधार पर भूगोल की तीन प्रमुख शाखाएँ हैं - भौतिक भूगोल, मानव भूगोल और जैव भूगोल।
भौतिक भूगोल में स्थलमंडल, वायुमंडल, जलमंडल और जीवमंडल का अध्ययन शामिल है।
वायुमंडल - वायुमंडल हवा की पतली परत है जो पृथ्वी को घेरे हुए है। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल वायुमंडल को अपने चारों ओर रखता है।
Tags:

Posted by: GKBIGBOSS
GKBIGBOSS सामान्य ज्ञान की साइट है जहाँ आप इतिहास, राजनीति, भूगोल, कंप्यूटर, विज्ञान, गणित, अर्थव्यवस्था, पर्यावरण और पारिस्थितिकी,समसामयिकी आदि के बारे में सामान्य ज्ञान सरल तरीके से प्राप्त करते हैं। यह साइट विभिन्न प्रतियोगी परिक्षाओं, स्कूल टीचरों एवं छात्रों और आम मानस के लिए बेहद उपयोगी है। डिजिटल युग में, ज्ञान की प्यास ऑनलाइन उपलब्ध जानकारी के विशाल महासागर से बुझती है। GKBIGBOSS दुनिया के बारे में अपनी समझ बढ़ाने की चाह रखने वालों के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में काम करती है।Popular Posts

जीव विज्ञान : एक सामान्य परिचय (Biology : A General Introduction)
रविवार, नवंबर 10, 2024

कंप्यूटर परीक्षण श्रृंखला 4 (COMPUTER MCQ TEST SERIES 4)
शनिवार, मई 18, 2024
CHILD DEVELOPMENT & PEDAGOGY
3/CHILD DEVELOPMENT & PEDAGOGY/post-list
Categories
- ANCIENT INDIA 2
- BIOLOGY 1
- BIOLOGY MCQ TEST 1
- BIOLOGY Q & A 1
- CHEMISTRY 1
- CHEMISTRY MCQ TEST 1
- CHEMISTRY Q & A 1
- CHILD DEVELOPMENT & PEDAGOGY 3
- CHILD DEVELOPMENT & PEDAGOGY ARTICLE 1
- CHILD DEVELOPMENT & PEDAGOGY MCQ 1
- CHILD DEVELOPMENT & PEDAGOGY Q & A 1
- COMPUTER 6
- COMPUTER ARTICLE 1
- COMPUTER MCQ TEST 4
- COMPUTER Q & A 1
- CURRENT AFFAIRS 2024 8
- ECONOMY 3
- ECONOMY ARTICLE 1
- ECONOMY MCQ TEST 1
- ECONOMY Q & A 1
- GEOGRAPHY 8
- GEOGRAPHY MCQ TEST 1
- HINDI 3
- HINDI ARTICLE 1
- HINDI MCQ TEST 1
- HINDI Q & A 1
- HISTORY 12
- HISTORY MCQ TEST 1
- HISTORY OF ANCIENT INDIA MCQ 1
- HISTORY OF ANCIENT INDIA Q & A 1
- HISTORY OF MEDIEVAL INDIA MCQ 1
- HISTORY OF MEDIEVAL INDIA Q & A 1
- HISTORY OF MODERN INDIA 1
- HISTORY OF MODERN INDIA MCQ 1
- HISTORY OF MODERN INDIA Q & A 1
- INDIA GEOGRAPHY 1
- INDIA GEOGRAPHY MCQ TEST 1
- INDIA GEOGRAPHY Q & A 1
- MEDIEVAL INDIA 1
- PHYSICS 1
- PHYSICS MCQ TEST 1
- PHYSICS Q & A 1
- POLITY 3
- POLITY ARTICLE 1
- POLITY MCQ TEST 1
- POLITY Q & A 1
- SCIENCE 11
- SCIENCE MCQ TEST 1
- TODAY IN HISTORY 3
- WORLD GEOGRAPHY 1
- WORLD GEOGRAPHY MCQ TEST 1
- WORLD GEOGRAPHY Q & A 1
- WORLD HISTORY MCQ 1
Random Posts
3/random/post-list
Recent in News
3/CURRENT AFFAIRS 2024/post-list
Popular Posts

जीव विज्ञान : एक सामान्य परिचय (Biology : A General Introduction)
रविवार, नवंबर 10, 2024

भौतिक विज्ञान प्रश्न उत्तर भाग 1 (Physics Question Answer Part 1)
रविवार, नवंबर 10, 2024

रसायन विज्ञान : एक सामान्य परिचय (Chemistry : A General Introduction)
रविवार, नवंबर 10, 2024

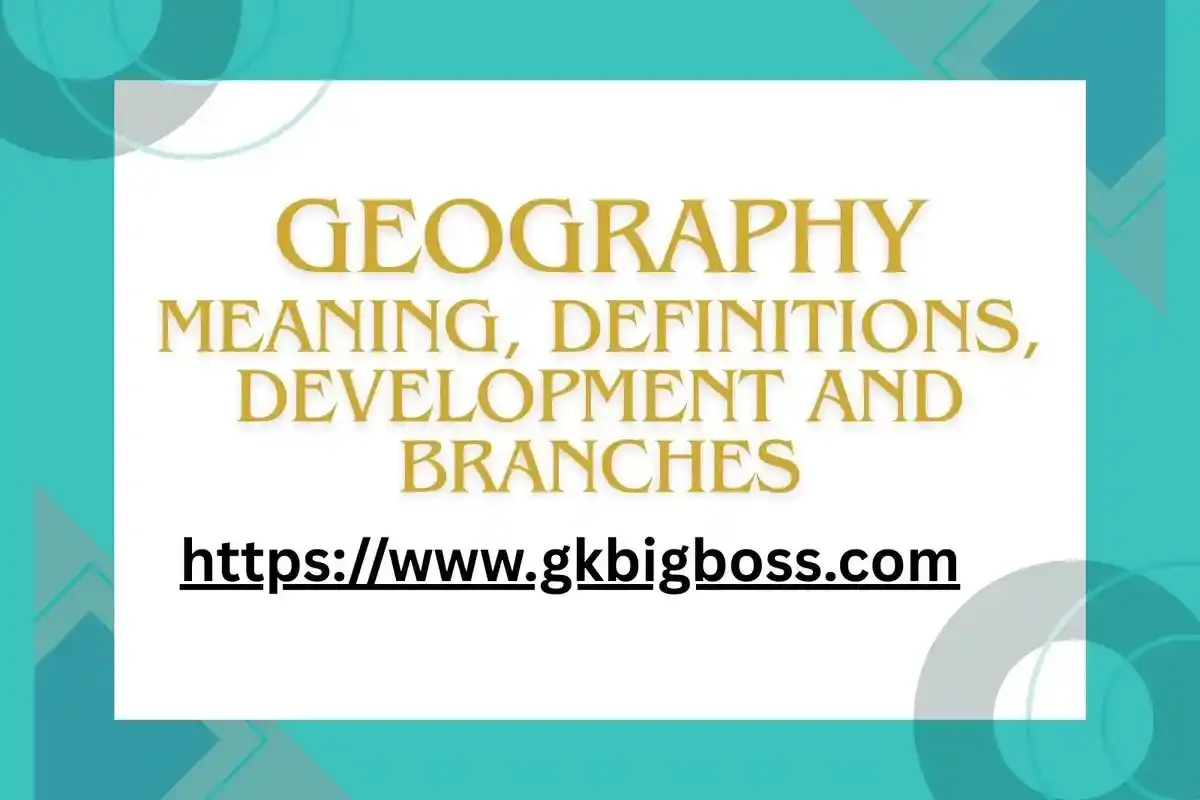

0 टिप्पणियाँ